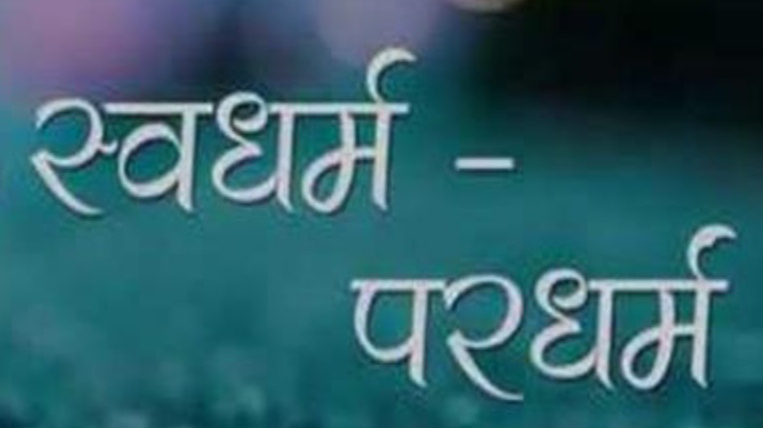नैरोबी सेक्टर में समाज आंदोलन
Shri P. R. Sarkar
नैरोबी सेक्टर(Nairobi Sector)
की समाज इकाइयों
(1) इबो — Ibo
(2) योरूबा — Yoruba
(3) ईडो — Edo
(4) गा — Ga
(5) हौसा — Hausa
(6) ईवे — Ewe
(7) ट्वी अकन — Twi Akan
(8) डियुला — Dioula
(9) बेटे — Bete
(10) बाकुला — Bacula
(11) मोसी — Mossi
(12) सेंगलेस — Sengales
(13) क्रियोलो — Criolo
(14) मेंडे — Mende
(15) टेम्ना — Temna
(16) पिग्मी — Pigmy
(17) लांडा — Landa
(18) हॉटेनटॉट — Hottentot
(19) ज़ुलु — Zulu
(20) डी-एन-शी — Di-N-Shi
(21) बगंडा — Baganda
(22) बुशमैन — Bushman
(23) होमा — Homa
(24) लोजी — Lozi
(25) न्यान्ज़ा — Nyanza
(26) स्वाहिली — Swahili
(27) अम्हारिक् — Amharic
(28) एओमो — Eomo
नैरोबी सेक्टर की समाज इकाइयों उत्तर से दक्षिण के क्रम में
(1) अम्हारिक् — Amharic (इथियोपिया - उत्तर-पूर्व)
(2) हौसा — Hausa (नाइजीरिया/नाइजर - सहेल क्षेत्र)
(3) मोसी — Mossi (बुर्किना फासो)
(4) सेंगलेस — Sengales (सेनेगल - पश्चिम अफ्रीका)
(5) डियुला — Dioula (माली/आइवरी कोस्ट)
(6) मेंडे — Mende (सिएरा लियोन)
(7) टेम्ना — Temna (सिएरा लियोन)
(8) क्रियोलो — Criolo (गिनी-बिसाऊ/केप वर्डे)
(9) योरूबा — Yoruba (नाइजीरिया/बेनिन)
(10) ईडो — Edo (नाइजीरिया)
(11) इबो — Ibo (नाइजीरिया)
(12) ट्वी अकन — Twi Akan (घाना)
(13) गा — Ga (घाना)
(14) ईवे — Ewe (घाना/टोगो)
(15) बेटे — Bete (आइवरी कोस्ट)
(16) एओमो — Eomo (ओरोमो - इथियोपिया/केन्या सीमा)
(17) बगंडा — Baganda (युगांडा)
(18) स्वाहिली — Swahili (केन्या/तंजानिया तटीय क्षेत्र)
(19) न्यान्ज़ा — Nyanza (केन्या/तंजानिया - विक्टोरिया झील क्षेत्र)
(20) बाकुला — Bacula (कांगो क्षेत्र)
(21) पिग्मी — Pigmy (मध्य अफ्रीका के वर्षावन)
(22) लांडा — Landa (लुंडा - अंगोला/कांगो/जाम्बिया)
(23) डी-एन-शी — Di-N-Shi (मध्य/दक्षिण-मध्य अफ्रीका)
(24) लोजी — Lozi (जाम्बिया/नामीबिया)
(25) होमा — Homa (नामीबिया/बोत्सवाना क्षेत्र)
(26) बुशमैन — Bushman (कालाहारी मरुस्थल - बोत्सवाना)
(27) हॉटेनटॉट — Hottentot (खोईखोई - नामीबिया/दक्षिण अफ्रीका)
(28) ज़ुलु — Zulu (दक्षिण अफ्रीका)
नैरोबी सेक्टर की समाज इकाइयों देशवार
पश्चिम अफ्रीका (West Africa)
नाइजीरिया (Nigeria): (1) इबो — Ibo
(2) योरूबा — Yoruba (3) ईडो — Edo
(4) हौसा — Hausa (नाइजर में भी)
घाना (Ghana):
(5) ट्वी अकन — Twi Akan
(6) गा — Ga
(7) ईवे — Ewe (टोगो में भी)
सिएरा लियोन (Sierra Leone):
(8) मेंडे — Mende
(9) टेम्ना — Temna
आइवरी कोस्ट / कोटे डी आइवर (Ivory Coast): (10) डियुला — Dioula (11) बेटे — Bete
सेनेगल (Senegal):
(12) सेंगलेस — Sengales
बुर्किना फासो (Burkina Faso):
(13) मोसी — Mossi
गिनी-बिसाऊ / केप वर्डे (Guinea-Bissau):
(14) क्रियोलो — Criolo
पूर्वी अफ्रीका (East Africa)
इथियोपिया (Ethiopia): (15) अम्हारिक् — Amharic
(16) एओमो — Eomo (ओरोमो)
युगांडा (Uganda):
(17) बगंडा — Baganda
केन्या और तंजानिया (Kenya & Tanzania): (18) स्वाहिली — Swahili (19) न्यान्ज़ा — Nyanza
मध्य अफ्रीका (Central Africa)
कांगो और आसपास के वर्षावन (Congo Basin): (20) पिग्मी — Pigmy (21) बाकुला — Bacula
अंगोला / कांगो (Angola/DRC):
(22) लांडा — Landa (लुंडा)
मध्य अफ्रीका क्षेत्र:
(23) डी-एन-शी — Di-N-Shi
दक्षिणी अफ्रीका (Southern Africa)
दक्षिण अफ्रीका (South Africa)
(24) ज़ुलु — Zulu
बोत्सवाना और नामीबिया (Botswana/Namibia): (25) बुशमैन — Bushman (सान)
(26) हॉटेनटॉट — Hottentot (खोईखोई) (27) होमा — Homa
जाम्बिया (Zambia):
(28) लोजी — Lozi
नैरोबी सेक्टर की
सामाजिक आर्थिक इकाई का
सामान्य परिचय
(1) इबो (Ibo/Igbo): दक्षिण-पूर्वी नाइजीरिया की प्रमुख इकाई। ये अपनी उद्यमिता और व्यापारिक कुशलता के लिए जाने जाते हैं।
(2) योरूबा (Yoruba): नाइजीरिया और बेनिन के निवासी। इनकी संस्कृति और नगरीय सभ्यता (Ifé) का इतिहास बहुत प्राचीन और समृद्ध है।
(3) ईडो (Edo): नाइजीरिया के बेनिन साम्राज्य से संबंधित। ये अपनी कलाकृति और कांस्य (Bronze) शिल्प के लिए प्रसिद्ध हैं।
(4) गा (Ga): मुख्य रूप से घाना की राजधानी अकरा और आसपास के तटीय क्षेत्रों के निवासी। ये पारंपरिक रूप से मछुआरे और व्यापारी रहे हैं।
(5) हौसा (Hausa): उत्तरी नाइजीरिया और नाइजर की विशाल इकाई। यह पूरे पश्चिम अफ्रीका में व्यापार और इस्लाम के प्रसार की मुख्य भाषा है।
(6) ईवे (Ewe): घाना, टोगो और बेनिन में फैली इकाई। ये अपनी जटिल बुनाई (Kente cloth) और संगीत के लिए जाने जाते हैं।
(7) ट्वी अकन (Twi Akan): घाना की सबसे बड़ी सांस्कृतिक इकाई। सोने के व्यापार और सशक्त राजनीतिक व्यवस्था (अशांति साम्राज्य) इनका इतिहास रहा है।
(8) डियुला (Dioula): यह एक व्यापारिक समुदाय है जो माली, आइवरी कोस्ट और बुर्किना फासो में फैला है। ये व्यापार और इस्लाम के वाहक रहे हैं।
(9) बेटे (Bete): आइवरी कोस्ट के निवासी। ये मुख्य रूप से कृषि (कोको और कॉफी) पर आधारित समाज हैं।
(10) बाकुला (Bacula): यह मुख्य रूप से कांगो क्षेत्र के समूहों से संबंधित है, जो अपनी स्थानीय कला और सामुदायिक जीवन के लिए जाने जाते हैं।
(11) मोसी (Mossi): बुर्किना फासो की प्रमुख इकाई। इनका इतिहास शक्तिशाली मोसी साम्राज्यों से जुड़ा है जो सदियों तक स्थिर रहे।
(12) सेंगलेस (Sengales): सेनेगल की मिश्रित सांस्कृतिक पहचान, जिसमें वोलोफ और अन्य समुदायों का प्रभाव है। यह फ्रेंच और स्थानीय भाषाओं का संगम है।
(13) क्रियोलो (Criolo): केप वर्डे और गिनी-बिसाऊ के मिश्रित अफ्रीकी-पुर्तगाली मूल के लोग। इनकी अपनी विशिष्ट भाषा और संस्कृति है।
(14) मेंडे (Mende): सिएरा लियोन की प्रमुख कृषि प्रधान इकाई। ये अपने गुप्त समाजों (जैसे Poro) और अनुष्ठानों के लिए जाने जाते हैं।
(15) टेम्ना (Temna): सिएरा लियोन के उत्तरी क्षेत्र की प्रमुख इकाई, जो खेती और व्यापार में सक्रिय है।
(16) पिग्मी (Pigmy): मध्य अफ्रीका के वर्षावनों के मूल निवासी। ये अपनी कम लंबाई और प्रकृति के साथ गहरे जुड़ाव (शिकार और संग्रहण) के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं।
(17) लांडा (Landa/Lunda): कांगो, अंगोला और जाम्बिया में फैले लोग। इनका अतीत महान लुंडा साम्राज्य से जुड़ा है।
(18) हॉटेनटॉट (Hottentot): इन्हें अब 'खोईखोई' कहा जाता है। ये दक्षिणी अफ्रीका के चरवाहे समूह हैं जिनकी भाषा में 'क्लिक' ध्वनियाँ होती हैं।
(19) ज़ुलु (Zulu): दक्षिण अफ्रीका की सबसे बड़ी और प्रसिद्ध योद्धा इकाई। राजा शाका ज़ुलु के नेतृत्व में इनका सैन्य इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है।
(20) डी-एन-शी (Di-N-Shi): मध्य अफ्रीका के आंतरिक क्षेत्रों की एक स्थानीय सांस्कृतिक इकाई।
(21) बगंडा (Baganda): युगांडा की सबसे बड़ी इकाई। इनके पास 'बुगांडा' नाम की अपनी राजशाही व्यवस्था है जो आज भी सांस्कृतिक रूप से सक्रिय है।
(22) बुशमैन (Bushman): इन्हें 'सान' भी कहा जाता है। ये कालाहारी मरुस्थल के प्राचीन निवासी हैं और शिकार की अद्भुत कला के लिए जाने जाते हैं।
(23) होमा (Homa): मुख्य रूप से नामीबिया और आसपास के क्षेत्रों से संबंधित एक छोटा भाषाई और सांस्कृतिक समूह।
(24) लोजी (Lozi): जाम्बिया के पश्चिमी प्रांत के निवासी। ये अपनी वार्षिक बाढ़ रस्म 'कुओम्बोका' के लिए प्रसिद्ध हैं।
(25) न्यान्ज़ा (Nyanza): विक्टोरिया झील के आसपास के लोग (जैसे लुओ)। इनका मुख्य व्यवसाय मछली पकड़ना और कृषि है।
(26) स्वाहिली (Swahili): पूर्वी अफ्रीका (केन्या-तंजानिया) के तटीय लोग। यह अरब और अफ्रीकी संस्कृति का मिश्रण है और इनकी भाषा पूरे अफ्रीका में प्रसिद्ध है।
(27) अम्हारिक् (Amharic): इथियोपिया की प्रमुख इकाई। यह इथियोपिया की आधिकारिक भाषा है और इसका संबंध प्राचीन ईसाई साम्राज्य से है।
(28) एओमो (Eomo/Oromo): इथियोपिया की सबसे बड़ी जातीय इकाई। इनकी अपनी प्राचीन लोकतांत्रिक सामाजिक व्यवस्था है जिसे 'गडा' (Gadaa) कहा जाता है।
ये सभी इकाइयाँ पी.आर. सरकार (P.R. Sarkar) द्वारा प्रतिपादित प्रउत (PROUT) दर्शन के अनुसार स्थानीय आर्थिक स्वावलंबन और सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण मानी गई हैं।
नैरोबी सेक्टर (अफ़्रीका) की सभी 28 इकाइयों के लिए प्रउत (PROUT) के सिद्धांतों पर आधारित
क्रमवार विकास योजना
इन सभी योजनाओं का मूल मंत्र है: "स्थानीय कच्चा माल, स्थानीय श्रम और स्थानीय उपभोग।"
पश्चिम अफ्रीकी ब्लॉक (West African Block)
(1) इबो (Ibo)
आर्थिक: 'सहकारी इंजीनियरिंग हब' की स्थापना। छोटे कल-पुर्जों और घरेलू उपकरणों के निर्माण में इनकी उद्यमशीलता का उपयोग।
सामाजिक: तकनीकी शिक्षा के लिए 'पीपल्स यूनिवर्सिटी' का निर्माण।
सांस्कृतिक: इबो साहित्य और लोक कला के संरक्षण हेतु डिजिटल आर्काइव।
(2) योरूबा (Yoruba)
आर्थिक: 'अदिरे' (वस्त्र) और कृषि-प्रसंस्करण इकाइयों का सहकारी नेटवर्क।
सामाजिक: शहरी नियोजन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की प्राथमिकता।
सांस्कृतिक: इनके प्राचीन नगरीय इतिहास और कला के लिए 'सांस्कृतिक विनिमय केंद्र'।
(3) ईडो (Edo)
आर्थिक: विश्व प्रसिद्ध कांस्य (Bronze) और धातु शिल्प का औद्योगिक स्तर पर सहकारी उत्पादन।
सामाजिक: शिल्पकारों के लिए सुरक्षित आवास और वृद्धावस्था पेंशन योजना।
सांस्कृतिक: बेनिन कला संग्रहालयों का स्थानीय संचालन।
(4) गा (Ga)
आर्थिक: समुद्री भोजन प्रसंस्करण और डिब्बाबंद मछली के निर्यात के लिए सहकारी इकाइयाँ।
सामाजिक: तटीय स्वच्छता और जल शुद्धिकरण परियोजनाओं का क्रियान्वयन।
सांस्कृतिक: 'होमोवो' उत्सव के माध्यम से सामुदायिक एकता का संचार।
(5) हौसा (Hausa)
आर्थिक: चमड़ा उद्योग और शुष्क अनाज (बाजरा-ज्वार) के लिए विशाल कृषि सहकारी समितियाँ।
सामाजिक: मोबाइल औषधालयों के माध्यम से दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा।
सांस्कृतिक: हौसा मौखिक परंपराओं और संगीत का संरक्षण।
(6) ईवे (Ewe)
आर्थिक: उच्च गुणवत्ता वाले हस्तशिल्प और संगीत वाद्ययंत्रों का निर्माण उद्योग।
सामाजिक: महिला सहकारी समितियों को वस्त्र उद्योग का नेतृत्व देना।
सांस्कृतिक: पारंपरिक नृत्य और संगीत के लिए अकादमियों की स्थापना।
(7) ट्वी अकन (Twi Akan)
आर्थिक: खनिज संसाधनों (सोना) का स्थानीय सहकारी स्वामित्व और लकड़ी उद्योग का सतत विकास।
सामाजिक: सभी के लिए बुनियादी शिक्षा और कौशल विकास।
सांस्कृतिक: 'असांते' गौरव और पारंपरिक शासन पद्धति का सम्मान।
(8) डियुला (Dioula)
आर्थिक: अंतर-क्षेत्रीय व्यापार के लिए सहकारी रसद (Logistics) और वेयरहाउसिंग।
सामाजिक: व्यापारियों और मजदूरों के लिए बीमा और सुरक्षा योजनाएँ।
सांस्कृतिक: व्यापारिक नैतिकता और भाषाई विविधता का संवर्धन।
(9) बेटे (Bete)
आर्थिक: कोको और कॉफी का शत-प्रतिशत स्थानीय प्रसंस्करण (चॉकलेट निर्माण)।
सामाजिक: कृषि मजदूरों के लिए मुफ्त चिकित्सा और शिक्षा।
सांस्कृतिक: कृषि आधारित उत्सवों और लोकगीतों का आयोजन।
(10) बाकुला (Bacula)
आर्थिक: सामुदायिक फल और सब्जी उत्पादन केंद्र।
सामाजिक: स्वच्छता और सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियान।
सांस्कृतिक: स्थानीय बोली और सामुदायिक रीति-रिवाजों का दस्तावेजीकरण।
(11) मोसी (Mossi)
आर्थिक: जल संचयन तकनीक और पशुधन आधारित डेयरी उद्योग।
सामाजिक: मृदा संरक्षण के लिए सामुदायिक वानिकी।
सांस्कृतिक: ऐतिहासिक मोसी साम्राज्य की न्यायप्रिय परंपराओं का पुनरुद्धार।
(12) सेंगलेस (Sengales)
आर्थिक: इको-पर्यटन और समुद्री व्यापार की सहकारी प्रबंधन प्रणाली।
सामाजिक: बेरोजगारी मिटाने के लिए कौशल विकास कार्यशालाएँ।
सांस्कृतिक: अफ्रीकी और वैश्विक संस्कृति के संगम का उत्सव।
(13) क्रियोलो (Criolo)
आर्थिक: समुद्री नमक उत्पादन और सौर ऊर्जा आधारित कुटीर उद्योग।
सामाजिक: द्वीपीय क्षेत्रों में संचार और परिवहन की सुदृढ़ व्यवस्था।
सांस्कृतिक: क्रियोल भाषा और संगीत के लिए विशेष शोध संस्थान।
(14) मेंडे (Mende)
आर्थिक: पाम ऑयल और प्राकृतिक फाइबर से निर्मित उत्पादों का उद्योग।
सामाजिक: ग्रामीण बुनियादी ढांचे (सड़क और बिजली) का विस्तार।
सांस्कृतिक: 'पोरो' जैसे पारंपरिक समाजों के नैतिक मूल्यों का उपयोग।
(15) टेम्ना (Temna)
आर्थिक: उन्नत चावल की खेती और भंडारण के लिए सामुदायिक साइलो (Silos)।
सामाजिक: किसानों के लिए सस्ती ऋण सुविधा और बीज बैंक।
सांस्कृतिक: स्थानीय कला और लोक कथाओं का स्कूलों में शिक्षण।
मध्य और पूर्वी अफ्रीकी ब्लॉक (Central & East African Block)
(16) पिग्मी (Pigmy)
आर्थिक: गैर-काष्ठ वन उत्पाद (शहद, औषधि) का सहकारी विपणन।
सामाजिक: उनके प्राकृतिक आवास (जंगल) के अधिकारों का संरक्षण।
सांस्कृतिक: उनके अद्वितीय जंगल कौशल और संगीत का विश्वव्यापी सम्मान।
(17) लांडा (Landa)
आर्थिक: तांबे और खनिजों के मूल्य-संवर्धन हेतु रिफाइनरी परियोजनाएँ।
सामाजिक: खदान क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण और स्वास्थ्य लाभ।
सांस्कृतिक: लांडा शाही परंपराओं का ऐतिहासिक संरक्षण।
(18) हॉटेनटॉट (Hottentot/Khoikhoi)
आर्थिक: भेड़ों की उन्नत नस्ल का पालन और ऊन आधारित वस्त्र इकाइयाँ।
सामाजिक: अर्ध-खानाबदोश समुदायों के लिए चल-स्कूल और अस्पताल।
सांस्कृतिक: 'क्लिक' भाषाओं के संरक्षण के लिए भाषाई शोध।
(19) ज़ुलु (Zulu)
आर्थिक: डेयरी उत्पादन और आधुनिक कृषि-फार्म सहकारी समितियाँ।
सामाजिक: युवाओं के लिए शारीरिक और सैन्य प्रशिक्षण अकादमियाँ।
सांस्कृतिक: ज़ुलु मार्शल आर्ट और पारंपरिक शिल्प का संवर्धन।
(20) डी-एन-शी (Di-N-Shi)
आर्थिक: बांस और स्थानीय लकड़ी से टिकाऊ फर्नीचर निर्माण।
सामाजिक: सामुदायिक स्वच्छता और पोषण सुरक्षा।
सांस्कृतिक: क्षेत्रीय बोलियों और लोक कला का प्रदर्शन।
(21) बगंडा (Baganda)
आर्थिक: केले के फाइबर से कागज़ और वस्त्र निर्माण के कारखाने।
सामाजिक: सुव्यवस्थित सामुदायिक प्रशासन और न्याय व्यवस्था।
सांस्कृतिक: लुगांडा भाषा और शाही संगीत का संरक्षण।
(22) बुशमैन (Bushman/San)
आर्थिक: पारिस्थितिकी-पर्यटन और पारंपरिक औषधियों का पेटेंट।
सामाजिक: जल संसाधनों तक स्थायी पहुँच सुनिश्चित करना।
सांस्कृतिक: उनके प्राचीन रॉक आर्ट और मरुस्थलीय ज्ञान का सम्मान।
(23) होमा (Homa)
आर्थिक: शुष्क भूमि खेती और छोटे पैमाने के सिंचाई प्रोजेक्ट।
सामाजिक: साक्षरता दर बढ़ाने के लिए प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम।
सांस्कृतिक: स्थानीय लोकगीतों का डिजिटल संरक्षण।
(24) लोजी (Lozi)
आर्थिक: बाढ़ के मैदानों में जलीय कृषि (Aquaculture) और धान की खेती।
सामाजिक: आपदा प्रबंधन और बाढ़ राहत के लिए स्थायी बुनियादी ढांचा।
सांस्कृतिक: 'कुओम्बोका' समारोह को वैश्विक पर्यटन से जोड़ना।
(25) न्यान्ज़ा (Nyanza)
आर्थिक: विक्टोरिया झील के किनारे मत्स्य पालन और कोल्ड स्टोरेज नेटवर्क।
सामाजिक: जलजनित रोगों के नियंत्रण हेतु स्वास्थ्य योजनाएँ।
सांस्कृतिक: झील के तट की पारंपरिक कहानियों और गीतों का संकलन।
(26) स्वाहिली (Swahili)
आर्थिक: मसालों का प्रसंस्करण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहकारी समितियाँ।
सामाजिक: तटीय शहरों में उच्च गुणवत्ता वाली नागरिक सुविधाएँ।
सांस्कृतिक: स्वाहिली भाषा को 'लिंगुआ फ्रेंका' के रूप में प्रउत साहित्य से जोड़ना।
(27) अम्हारिक् (Amharic)
आर्थिक: उच्च भूमि कृषि, कॉफी उत्पादन और निर्यात सहकारी केंद्र।
सामाजिक: आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ पारंपरिक चिकित्सा का एकीकरण।
सांस्कृतिक: प्राचीन गीज़ (Ge'ez) लिपि और ऑर्थोडॉक्स कला का संरक्षण।
(28) एओमो (Eomo/Oromo)
आर्थिक: बड़े पैमाने पर पशुपालन और अनाज उत्पादन सहकारी समितियाँ।
सामाजिक: 'गडा' (Gadaa) प्रणाली को सहभागी लोकतंत्र के रूप में लागू करना।
सांस्कृतिक: ओरोमो भाषा के साहित्य और पारंपरिक खेलों का विकास।
करण सिंह राजपुरोहित जी, यह प्लान प्रउत के "आत्मनिर्भर आर्थिक इकाइयों" के सपने को साकार करने की दिशा में एक रूपरेखा है।
ये सभी प्रोजेक्ट्स "सबकी न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी" के प्रउतवादी सिद्धांत पर आधारित हैं।
प्रउत (PROUT) के सिद्धांतों के आधार पर
उदाहरण के लिए
पिग्मी सामाजिक-आर्थिक इकाई
के लिए मास्टर प्लान
1. आर्थिक मास्टर प्लान (Economic Blueprint)
इसका मुख्य लक्ष्य 'पूंजी का केंद्रीकरण' रोकना और स्थानीय संसाधनों पर स्थानीय नियंत्रण करना है।
वन-आधारित सहकारी समितियाँ : लकड़ी काटे बिना (Non-Timber Forest Products) शहद, औषधीय पौधों, मशरूम और प्राकृतिक रबर के संग्रहण और प्रसंस्करण के लिए सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।
मूल्य संवर्धन (Value Addition): कच्चे माल को बाहर बेचने के बजाय, पिग्मी क्षेत्रों में ही छोटी औषधीय अर्क इकाइयां (Processing Units) स्थापित की जाएंगी ताकि लाभ का बड़ा हिस्सा वहीं रहे।
भूमि अधिकार और कृषि: इन्हें वर्षावनों के भीतर 'एग्रो-फॉरेस्ट्री' (वन-खेती) के लिए सुरक्षित भूमि आवंटित की जाएगी, जहाँ ये अपनी पारंपरिक जीवनशैली के साथ सात्विक खेती कर सकें।
2. सामाजिक मास्टर प्लान (Social Blueprint)
इसका लक्ष्य 'न्यूनतम आवश्यकताओं की गारंटी' देना है।
आवास और स्वास्थ्य : वर्षावनों के अनुकूल, पर्यावरण-हितैषी आधुनिक आवास और 'चल-चिकित्सालय' (Mobile Clinics) जो स्थानीय जड़ी-बूटियों और आधुनिक चिकित्सा का संगम हों।
शिक्षा : पिग्मी बच्चों के लिए ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो उनकी वन-विद्या को भी मान्यता दे और उन्हें आधुनिक विज्ञान से भी जोड़े।
शोषण से मुक्ति : बिचौलियों को पूरी तरह समाप्त कर सीधे सहकारी विपणन प्रणाली (Direct Marketing) लागू करना।
3. सांस्कृतिक मास्टर प्लान (Cultural Blueprint)
इसका लक्ष्य 'सांस्कृतिक विरासत' का संरक्षण और विकास है।
भाषा और संगीत का संरक्षण : पिग्मी संगीत और उनकी अद्वितीय मौखिक परंपराओं को डिजिटल रूप में संरक्षित करना और उन्हें वैश्विक पहचान दिलाना।
सांस्कृतिक पर्यटन (Eco-Tourism): पर्यटन को केवल व्यावसायिक न रखकर 'सांस्कृतिक विनिमय' बनाना, जहाँ लोग पिग्मी समुदाय से प्रकृति के साथ संतुलन में रहना सीख सकें।
4. सदविप्र राज स्थापना (Establishment of Sadvipra Leadership)
प्रउत का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ नैतिक नेतृत्व है।
स्थानीय बोर्ड का गठन : पिग्मी समुदाय के भीतर से ही उन व्यक्तियों को चुनना जो नैतिक रूप से सुदृढ़, निस्वार्थ और सेवाभावी हों। इन्हें 'सदविप्र' के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।
निगरानी समिति : ये सदविप्र यह सुनिश्चित करेंगे कि सहकारी समितियों में किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार न हो और आर्थिक लाभ का वितरण न्यायसंगत (Rational Distribution) हो।
जागरूकता केंद्र : सदविप्रों द्वारा संचालित केंद्र जो समुदाय को उनके अधिकारों और शोषण के प्रति जागरूक करेंगे।
निष्कर्ष: यह मास्टर प्लान पिग्मी समुदाय को केवल "मदद" देने के बजाय उन्हें अपनी अर्थव्यवस्था का "मालिक" बनाने पर केंद्रित है। जब समाज के सबसे अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति स्वावलंबी होगा, तभी नैरोबी सेक्टर में वास्तविक प्रउत की स्थापना होगी।
करण सिंह राजपुरोहित
प्रकाशन सचिव
प्राउटिस्ट सर्व समाज
9982322405