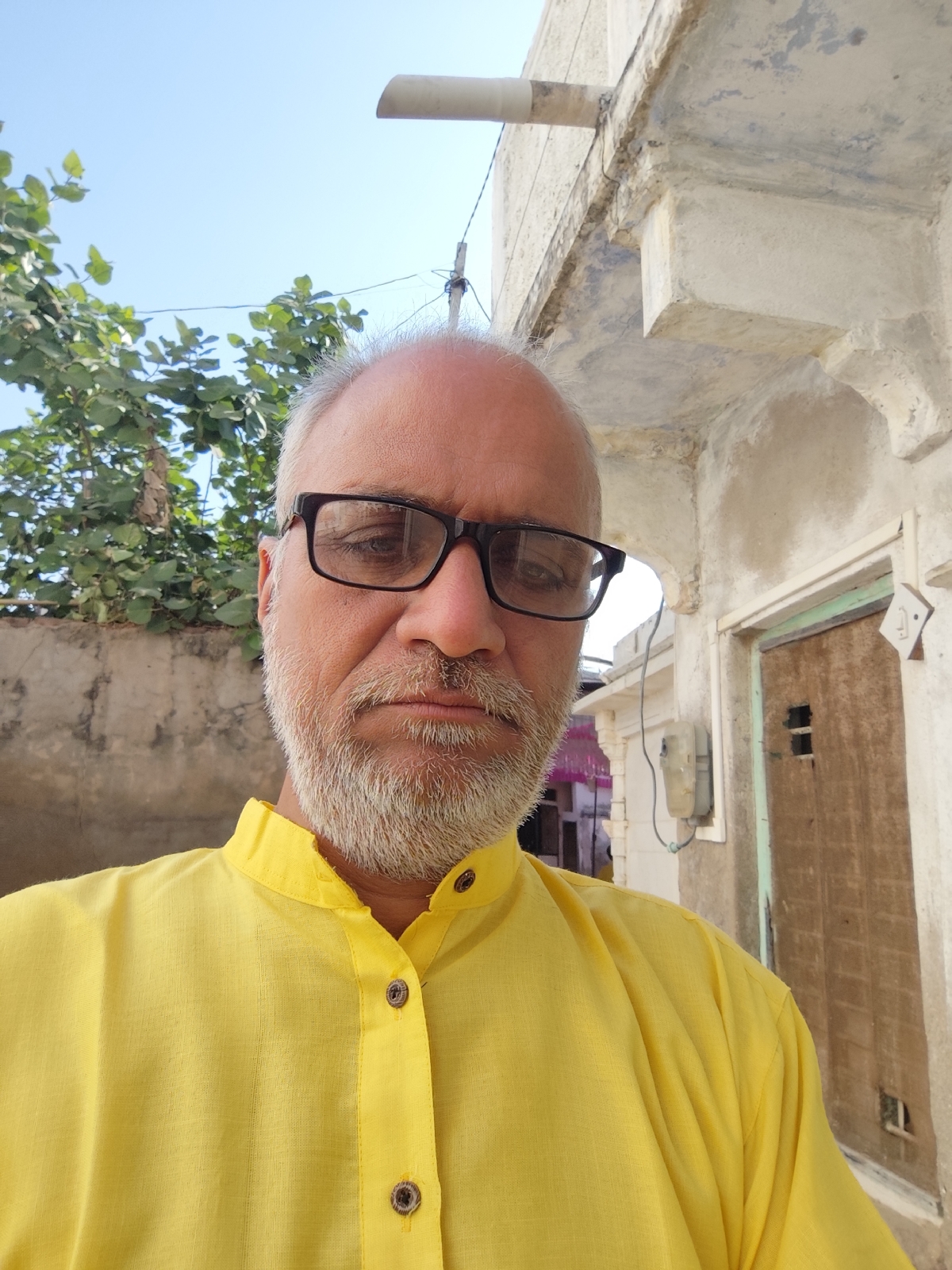-------------------------------------
आनन्द किरण
-------------------------------------
मनुष्य का जीवन निर्माण की आधारशिला यम-नियम है। जब तक मनुष्य को यम-नियम के पालन का पाठ नहीं पढ़ाया जाता है, तब तक मनुष्य के निर्माण के सभी दावे खोखले है। अतः मनुष्य के जीवन अथवा चरित्र निर्माण पर काम करने वालों को उनका बुनियादी पाठ्यक्रम (basic course) में यम-नियम को स्थापित करना चाहिए। इसके बिना मनुष्य को कोई भी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं धार्मिक जिम्मेदारी देने का अर्थ है कि जानबूझकर समाज को रसातल की ओर ले जाना है। इसलिए अब प्रश्न उठ रहा है कि यम-नियम क्या है?
यम-नियम एक विधा है, जो मनुष्य के जीवन निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यदि दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके बिना मनुष्य का निर्माण असंभव है। इसलिए आज हम यम-नियम की शिक्षा पाएंगे।
यम, मनुष्य के अंदर के उन संवेगों का नियंत्रण की शिक्षा देता है, जो मनुष्य को पशुत्व से प्राप्त हुए हैं, अथवा पशुत्व की ओर ले जाते हैं। सरल अर्थ में कहा जाए तो यम, मनुष्य के अंदर पाश्विक संवेगों को मानवीय संवेगों में बदलने की कला का नाम है। इसको उदाहरण द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। हिंसा मनुष्य के अंदर पाश्विक जगत से आती है, यदि यह मनुष्य में यथावत बनी रहती है तो यह मनुष्य को न केवल पशु बनाती है अपितु पशु से अधम असुर, दानव, राक्षस, दैत्य, हैवान, शैतान एवं पिशाच बना सकती है। अतः मनुष्य अपने मनुष्यत्व से गिर जाता है, इसलिए अहिंसा प्रथम यम बनकर मनुष्य को पशुत्व की श्रेणी में जाने से रोकता है। दूसरा यम सत्य है। असत्य अथवा झूठ की दुनिया में मनुष्य को जीवन खोखला तथा चरित्र अव्यवहारिक बनकर उभरता है, इसलिए सत्य उस पर पहरा बिठा दिया है ताकि मनुष्य अवास्तविक बनकर नहीं रह जाए। तीसरा यम अस्तेय है, जो मनुष्य को चौर्य वृत्ति से दूर रखता है। चोरी करना सामाजिक एवं वैधानिक अपराध है। यह मनुष्य में लालस के कारण जन्म लेता है तथा मनुष्य की सम्पूर्ण प्रतिष्ठा को धूमिल कर देते हैं। अतः अस्तेय अर्थात चोरी नहीं करने की शिक्षा मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है। व्यर्थ के चिन्तन से बचने के लिए चतुर्थ यम के रूप में ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। ब्रह्मचर्य का अर्थ मन को ब्रह्म भाव में रत रखना है। इसके अभाव में व्यर्थ एवं अवांछित चिन्तन की ओर ले जाती है। अपरिग्रह का अर्थ आवश्यक से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करने के नाम है। अपरिग्रह मनुष्य को सामाजिक प्राणी के रूप में स्थापित करने की एक मजबूत विधा है। इसलिए पांचवे यम के रूप में मनुष्य को अपरिग्रह की शिक्षा दी जाती है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह का संयुक्त नाम यम है। अतः यम, सामाजिक शुचिता बनाये रखने तथा मनुष्य में दैवीय गुणों के विकास के लिए आध्यात्मिक पाठशाला में नैतिकता के प्रथम पाठ के रूप में पढ़ाया जाता है। यम का संबंध मन, वचन एवं कर्म तीनों की विधा से है। यद्यपि वैधानिक जगत में कर्म में परिणित को ही अपराध की श्रेणी में रखा गया है तथापि वचन से उत्पन्न अशुचिता सामाजिक दृष्टि में बुराई अथवा अन्याय कर्म में रखा गया है। मन के अंदर उत्पन्न यम विरोधी तत्व को आध्यात्मिक, नैतिक एवं धार्मिक दृष्टि पाप की श्रेणी में गण्य है। यद्यपि मन में उत्पन्न हिंसा, झूठ, चौर्य भाव, व्यर्थ चिन्तन एवं परिग्रह वृत्ति समाज की क्षति नहीं करते हैं तथापि मनुष्य के व्यक्तित्व निर्माण में बाधक है तथा मनुष्य की ब्रह्मत्व प्राप्ति की यात्रा में अवरोध पैदा करते हैं। अतः यम-नियम विरोधी आचरण पाप है।
यम को शास्त्र में मृत्यु का देवता बताया गया है। जबकि यम विधा के रूप में मनुष्य को मनुष्यत्व, दैवत्व, ईश्वरत्व एवं ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित करने की यात्रा का प्रथम द्वार है। अतः शास्त्र एवं विज्ञान के भाव को समझना बहुत जरूरी है। शास्त्र का यमराज एक धर्मराज भी है, जो मनुष्य के कर्मों का हिसाब करता है। हम जानते हैं कि धर्म मनुष्य को सत्पथ पर ले चलाता है। अतः यम अमंगल का प्रतीक नहीं अपितु जीवन का प्रथम एवं अन्तिम सत्य है। यम के बिना मनुष्य ही नहीं रहता है। अतः यम की शरण में मनुष्य को जाने से डर नहीं है, यम से वह डरता है, जिसको मनुष्योचित कर्म करने में भय है। जो जीवन भर यम से पृथक रहकर चलता है, उसे मृत्यु के बाद यम का हिसाब देने के लिए यमराज मृत्यु के देवता के रूप में स्थापित किया है। अर्थात यह बताया गया है कि मनुष्य के यम से बचने का कोई उपाय नहीं है। अतः बुद्धिमान मनुष्य जीवन भर यम को मानकर चलता है।
नियम मनुष्य परिवेश से प्राप्त अवांछित कृत्य के हाथों सुरक्षात्मक उपाय है। शौच मनुष्य को गंदगी फैलाने से बचाता है तथा स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर ले चलता है। संतोष मनुष्य को तृष्णा व अतृप्ति से बचाकर संतुष्टि, शांति एवं आनन्द की ओर ले चलता है। तप मनुष्य को गैरजिम्मेदार एवं निष्ठुरता से बचाकर मानवीय संवेदना की ओर ले चलता है। इसी प्रकार स्वाध्याय मनुष्य को सत्पथ की निर्देशना देता है तथा ईश्वर प्रणिधान मनुष्य को ईश्वरत्व प्राप्ति की ओर ले चलता है। इस प्रकार नियम के बल पर मनुष्य बाहरी अच्छाइयों को ग्रहण करता है तथा बुराइयों को अंदर प्रवेश नहीं कर देने की शिक्षा पाता है।
मनुष्य के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के प्रति सजग रहने के लिए शौच को प्रथम नियम के रूप स्थापित किया है, संतोष की द्वितीय नियम में रुप में तृप्ति की ओर ले जाकर तड़पन एवं बैचेनी से बचाती है। इस प्रकार शौच शारीरिक, मानसिक स्वच्छता के लिए है तो संतोष सम्पूर्ण रूप से मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए। तप मनुष्य का मानसाध्यात्मिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता को सुरक्षित करता है। अर्थात मनुष्य साधुत्व का पाठ पढ़ाता है। दूसरों का दु:ख देखकर जिसका दिल द्रवित नहीं होता, वह मनुष्य कहलाने से चूक जाता है। इसलिए तृतीय नियम के रूप तप की शिक्षा दी जाती है। स्वाध्याय को चतुर्थ नियम बताया गया है, यह सत्पथ की निर्देशना के लिए आवश्यक है, इसके अभाव में मनुष्य के सत्य-असत्य, न्याय-अन्याय, नीति-अनीति तथा धर्म-अधर्म में भेद करना असंभव हो जाता है। अतः स्वाध्याय को नियमित अभ्यास के रूप में स्थापित किया है। अतः आध्यात्मिक मानसिक की स्वच्छता एवं स्वस्थता के लिए आवश्यक है। इसके अभाव में मनुष्य अधर्म को धर्म तथा धर्म को धर्म नहीं समझ सकता है। ईश्वर प्रणिधान पंचम नियम के रूप में मनुष्य को पूर्णत्व की प्राप्ति की ओर ले चलता है। बिना पूर्णत्व के मनुष्य अपना जीवन उद्देश्य सफल नहीं कर सकता है। अतः ईश्वर प्रणिधान मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक है। यह आध्यात्मिक स्वच्छता के लिए आवश्यक है।
नोट - यम-नियम की शिक्षा लेने के लिए श्री श्री आनन्दमूर्ति जी कृति जीवन वेद को पढ़े।